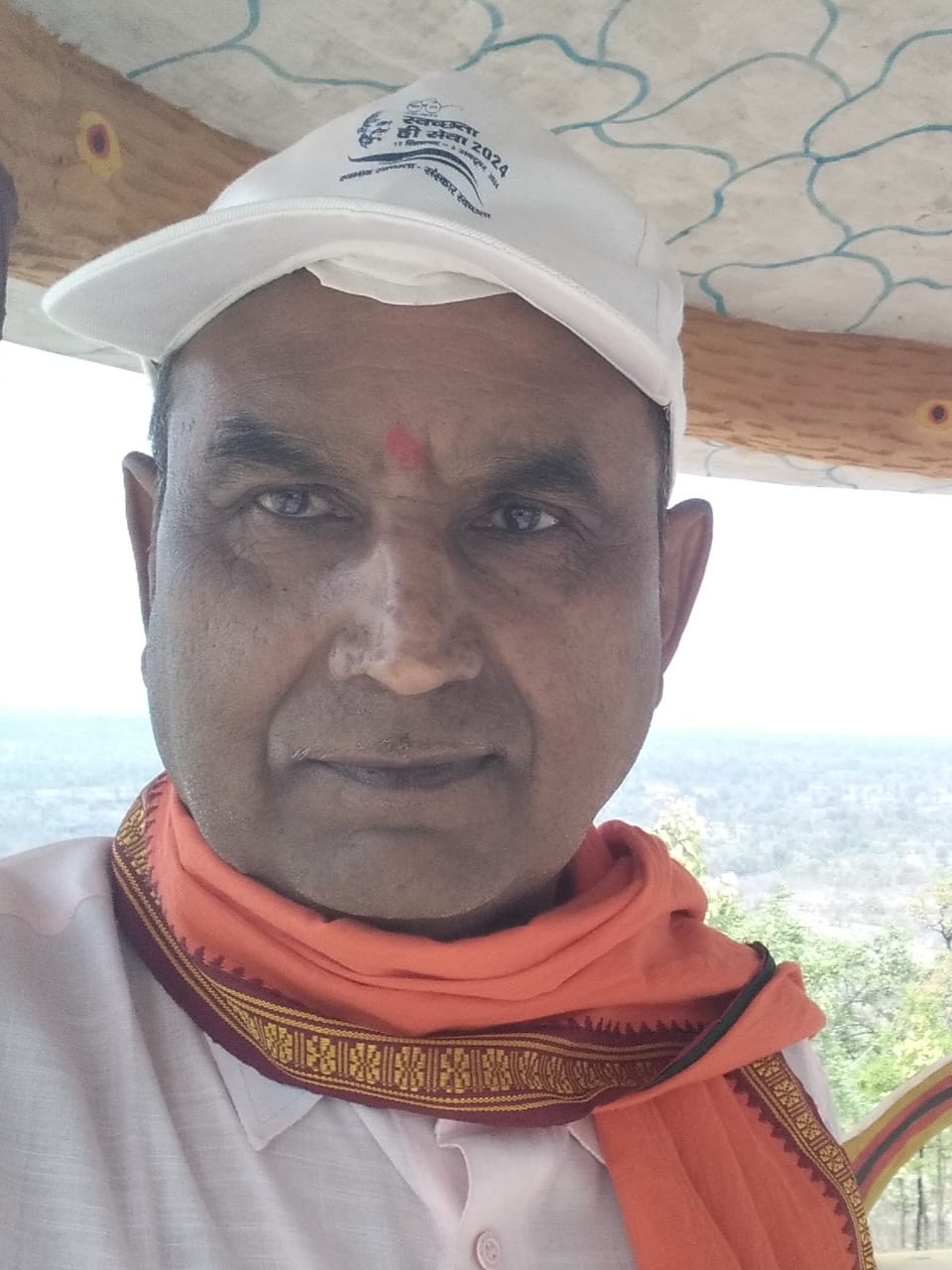
क्यों लुप्त हो रही हैं सावन भादो की खुशियां ?
पर्यावरण एवं प्रकृति चिंतन-क्र.17 बीरेन्द्र श्रीवास्तव की कलम से
एमसीबी। परिवर्तन जीवन और प्रकृति का वह पक्ष है जो नवीनता को आमंत्रण देता है. यही कारण है की ऋतु परिवर्तन पूरी धरती को नए-नए रंगों में भिगोकर अलग-अलग रूप में प्रस्तुत करती रहती है जिसे देखकर प्रकृति का अंग अंग चाहे वह पेड़ पौधे हो पशु पक्षी हो या मानव जीवन सभी एक नए बदलाव की खुशी का एहसास करते हैं. कहा जाता है कि बिना परिवर्तन जीवन नीरस और स्थिर हो जाता है. नए-नए परिवर्तन में साक्षात्कार साक्षात्कार कराती प्रकृति जीवन को और जीने की ललक पैदा करती है. इसीलिए ईश्वरी शक्ति द्वारा प्रदत्त इस प्रकृति ने अलग-अलग रंगों में अलग-अलग ऋतुओं का उपहार हमें प्रदान किया है ताकि जीवन नीरसता से आगे उमंग और खुशियों से सराबोर होकर और जीवन जीने के लिए लालायित रहे.
पृथ्वी ने अपने विशाल आंचल में फैले प्राकृतिक जंगल पेड़ पौधे और फूलों के रंग के साथ-साथ वाय,जल, नदियां, बर्फ के पहाड़ और झीलों का सौंदर्य देकर सभी का अलग-अलग नामकरण कर दिया है, जिसे हम अपनी भाषा में राष्ट्र या देश के नाम से जानते हैं इसमें रहने वाले पशु पक्षी एवं मानव रंग रूप में भले ही अलग दिखाई देते हैं किंतु खुशियों की एक ही परिभाषा होती है जो सभी के चेहरे पर या मन में दिखाई पड़ती है कभी-कभी यही खुशी शब्दों में बांधकर गीतों का स्थान पाती है और कभी हमारे शरीर की धड़कन एवं गुनगुनाने की भावाविभक्ति गायन वादन और नृत्य के रूप में दिखाई पड़ता है हर देश हर व्यक्ति और समूह इसे अपने भाव के अनुरूप व्यक्ति व्यक्त करने की कोशिश करता है जो स्थिर जीवन को गति प्रदान करती है ऋतुओं का यह परिवर्तन हमारे जीवन के सुख-दुख का परिचायक भी है हमारे देश में शरद, वर्षा और ग्रीष्म तीन ऋतु मुख्य रूप से जानी जाती है लेकिन अपनी खुशियों को परिवर्तन से जोड़ते हुए हमने बसंत, शिशिर और हेमंत जैसी ऋतुओं का सृजन कर लिया है. हमारे गांव का लोक जीवन इसे अलग-अलग महीनो में बांटकर उत्सव का आनंद लेते रहे हैं. चैती, होरी, कजरी, झूला गीत, बारहमासा, बासंती, और तीज के साथ बघेली पाई और छठ के गीत अलग-अलग अवसरों पर जीवन को उत्साह और आनंद देने के लिए गए जाते हैं.

सूरज की गर्मी जब धीरे-धीरे बढ़ते हुए अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचने लगती है तब चिंतित हम आपसी बातचीत में कहते लगते हैं कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है जाने कब तक पानी बरसेगा. लेकिन गर्मी ज्यादा है कहने से पानी नहीं बरसता है. छुटपुट पानी की बूंदे धरती की तपन को कम नहीं कर सकती. नौतपा की गर्मी के बाद हम आषाढ़ मास की बारिश का इंतजार करने लगते हैं. इसी आषाढ़ का पानी धरती को छूते ही किसानों को आशावादी बना देता है. बच्चों को बरबस हाथ में पानी की बूंदे लेने की खुशी और बारिश में भीगने का आनंद लेने हेतु लालायित करता है. युवा मन को यही पानी भीगकर खुद को देखने और दिखाने का आमंत्रण देने लगता है. यही बूंदे अपने भावों को अलग-अलग विधाओं में अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित करती है कवियों को गीत लिखने तथा कलाकार को कूंची में रंग भरने हेतु बाध्य कर देती है और धीरे धीरे बारिश के साथ हंसते खिलखिलाते बारिश में नहाए पेड़ पौधे, नदी , पहाड़ , बच्चों का पानी में भीगा बालपन,यौवन की उभरती अभिलाषा और स्वर लहरियो के आलाप के साथ तान छेड़ते किसी कलाकार की सुर, लय, तान की भावना भरे शब्दों के साथ बिखरती खुशियों के चित्र और प्रतिबिंब उभरने लगते हैं.
लेखक मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन पुस्तक में इसी आषाढ़ की नायिका की खुशियों को शब्द देकर साहित्य में वह स्थान बना लिया जो लोगों को कम ही मिल पाता है. आषाढ़ से आगे सावन और भादो का महीना तो मानो उत्सव की टोकरी भरकर हमारे सामने उड़ेलने के लिए तैयार दिखाई देता है. खुशियों का अंबार देख मन उतावला हो जाता है और लोकगीत कजरी और झूला और मल्हार के गीतों की स्वर लहरियों में मन की बात कहने व्याकुल हो जाता है. बारिश में भीगने का आनंद ही अलग है. सत्य यही है कि बारिश मे बिना भीगे शब्दों और लेखन के महारथी कालिदास के श्रृंगार रस में डूबी मेघदूत के यक्ष की पीड़ा और प्रेयसी को भेजे संदेश की गहराइयों को समझा नहीं जा सकता.
सावन में लोक गीतों की गहराई में डूबे प्रकृति के संगीत में मानव के प्रेम, आनंद वियोग और सामाजिक उल्लास का अनोखा संगम दिखाई पड़ता है. सावन के झूले की पटेंग के साथ महिलाओं के गीतों की पंक्तियां हवाओं में बिखरकर उनकी खुशियों का इजहार करती है. भारत के पूर्वांचल में गाया जाने वाले कजरी और मल्हार के गीत लोकगीतों को वह ऊंचाइयां दे चुके हैं जो आज भी सुनते हुए आप आप झूम जाएंगे. यही कारण है कि हमारी इसी सांस्कृतिक पहचान को जीवंत रखने वाले इसके गायको कोदेश के पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया है. इस परंपरा में शारदा सिन्हा, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर और पंडित छन्नूलाल मिश्र का नाम अग्रणी आता है. कजरी जैसे लोकगीत के लिए शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण तथा गिरिजा देवी को पद्मश्री और कजरी के संरक्षण के लिए अजीता श्रीवास्तव को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है. लोकगीत हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जो हमारे देश की पहचान का प्रतिनिधित्व करती है.
प्राचीन काल से ही सभी ऋतुओं को मानव मन से जोड़ा गया है यही कारण है कि संस्कृत के कवियों से लेकर वर्तमान हिंदी के कवियों ने वर्षा के बारे में अपनी कलम के शब्दो से अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश की है. संस्कृत कवि शूद्रक, भतृहरी, जयदेव, महाकवि कालिदास और माघ ने वर्षा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है . कालीदास के मेघदूत मैं वर्षा ऋतु और प्रकृति के के हर रूप का वर्णन जितना डूब कर किया गया है वह शायद अब देखने को नहीं मिलेगा. तुलसीदास ने स्वयं राम के मुख से लक्ष्मण के माध्यम से किष्किंधा कांड में वर्षा को व्यक्त किया है “वर्षा काल मेघ घन छाए, गरजत लागत परम सुहाए”. इसी तरह रहीम ने लिखा है कि “पावस देखि रहीम मन कोईल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भए हमको पूछे कौन”. जयशंकर प्रसाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और प्रकृति के कवि सुमित्रानंदन पंत ने वर्षा की झरती बिखरती बूंदो पर अपने लेखन का सर्वस्व निछावर कर दिया है ,जिसमें उन्होंने पावस ऋतु को अलग-अलग संदर्भ में पूरी तरह जिया है.
वर्षा ऋतु की खुशियां मूक खड़े जंगल पहाड़, के साथ जीव जंतु और पशु पक्षी भी अपनी-अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं. बारिश की बूंदे अपने आसपास के पहाड़ों और नदियों का मधुर संगीत सुनने और साल भर से धूल में सने पहाड़ों को वर्षा जल से जब नहला दूल्हा कर मनमोहन रूप प्रदान करती है तब आप उसे देखकर खुशियों से “वाह कितना सुन्दर” कहने के लिए बाध्य हो जाते हैं. जी हां आपकी तरह ही यह जंगल पहाड़ और प्रकृति का हर कोना वर्षा की बूंदों का आभार प्रकट करता है. नदियाँ वर्षा का जल लेकर इतनी तेज भागती है मानो कोई उनसे यह वर्षा का जल भंडार छीनने की कोशिश कर रहा हो. नदियाँ इसी वर्षा जल से अपने ऊपर हुए अतिक्रमण, कूड़ा करकट और गंदगी की को बाहों में समेट कर समुद्र में ले जाकर डाल देती है और अपनी पवित्रता सहित श्वेत परिधान का वरण कर प्रसन्न होती है. सत्य यही है कि मानव प्रकृति के साथ रहकर ही आगे बढ़ सकता है.आनंद और उत्साह का रास्ता ही जीवन को गति प्रदान करता है. मानव के लिए विकास के नाम पर प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ का परिणाम ही उसे विध्वंसकारी बना रहा है अन्यथा प्रकृति तो हमारी जीवन दायिनी है हमारे दुख सुख मे शामिल प्रकृति विध्वंसकारी कैसे हो सकती है. कश्मीर और उत्तराखंड के भूस्खलन तथा नदियों का प्रचंड वेग हमें बार-बार चेतावनी दे रहा है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर ही हमें आगे बढ़ना होगा. उसके गीतों और स्वरों को सुनना होगा अन्यथा ऋतुए हमारा साथ छोड़ देंगी. वर्षा का पानी भी हमसे दूर होने लगेगा. हमारी चिंता यह होनी चाहिए कि प्रकृति के गीत चुप ना हो, उन्हें किसी की नजर ना लगे, क्योंकि यही प्रकृति हमारी जीवन रेखा है.
समय के परिवर्तन एवं बाजारवाद की दुनिया में अधाधुंध धन कमाने की होड़ हमारी खुशियों पर ग्रहण लगा रही हैं. जीवन का उल्लास और खुशियां अब धनार्जन के संघर्ष में कैद होने लगे हैं. लोक जीवन का संगीत और शब्दों को महसूस करने के लिए आज हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आर्थिक तराजू पर यदि हम खुशियां को धन से तौलने की कोशिश करेंगे तब निश्चित ही खुशियों का पलड़ा भारी होगा. हमारी संस्कृति के अंग हमारे ऋतु, हमारे लोकगीत की मिठास और आनंद का लुप्त होना, हमारी चिंता में अब शामिल होना चाहिए अन्यथा हमारे जीवन की गति धीरे-धीरे कब समाप्त हो जाएगी यह हमें पता भी नहीं चलेगा.
राजेश सिन्हा 8319654988







